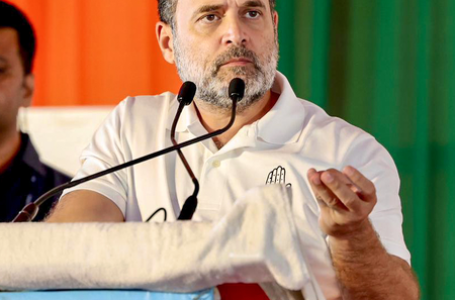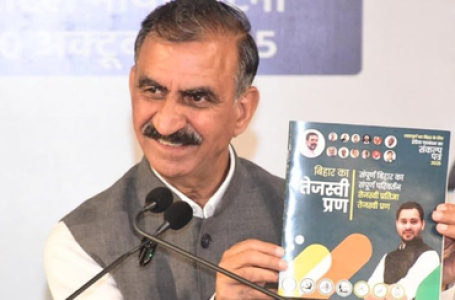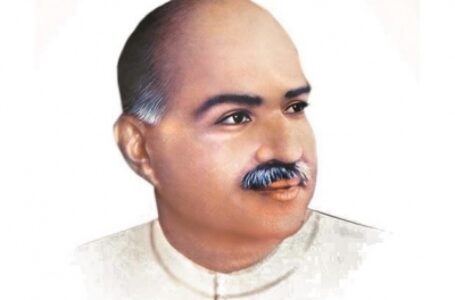बीजिंग । दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा प्रणालियां अभूतपूर्व दबाव का सामना कर रही हैं। बढ़ती उम्र की आबादी, पुरानी बीमारियों का बोझ और सीमित चिकित्सा संसाधनों की वजह से अधिकांश देश जूझ रहे हैं। इन चुनौतियों के बीच, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) उम्मीद की एक नई किरण बनकर उभरा है, जो न केवल इलाज को बेहतर बना सकता है, बल्कि इसे ज्यादा सुलभ और सटीक भी बना रहा है।
चीन की बात करें तो यहां स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि 2035 तक देश की लगभग एक-तिहाई आबादी 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की हो जाएगी। ऐसे में एआई आधारित तकनीकों का उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक निर्णायक कदम बनता जा रहा है।
आज चीन के कई अस्पतालों और विशेष जांच केंद्रों में आधुनिक एआई डायग्नोस्टिक सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं। यह तकनीक खासकर उन इलाकों में बेहद कारगर साबित हो रही है जहां डॉक्टरों की भारी कमी है। उदाहरण के तौर पर, ग्रामीण चीन में एआई-आधारित दूरस्थ डायग्नोसिस सिस्टम ने गलत बीमारी पहचान की दर को 63 प्रतिशत तक कम कर दिया है। यह न केवल रोगियों की जान बचा रहा है, बल्कि डॉक्टरों का काम भी आसान बना रहा है।
शहरी अस्पतालों में भी एआई का असर देखा जा रहा है। जैसे चोंगशान अस्पताल में, जहां केवल 136 डॉक्टरों को सालाना 8.2 लाख ओपीडी मरीजों की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। वहां एआई का इस्तेमाल हृदय रोगों की सटीक पहचान और इलाज में हो रहा है। वहीं, छोटे शहरों के अस्पताल भी पीछे नहीं हैं। चच्यांग प्रांत के वूज़न शहर के अस्पताल ने एआई की मदद से हजारों मरीजों को बेहतर सेवाएं दी हैं।
चीन की सरकार भी राष्ट्रीय स्तर पर “एआई प्लस” जैसी पहलों के जरिए तकनीक और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच की दूरी को पाटने में जुटी है। शांगहाई में दवा विकास और क्लिनिकल निर्णयों में एआई के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि इलाज के नतीजे और ज्यादा प्रभावी हो सकें।
चीन अकेला देश नहीं है जो एआई के ज़रिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने में जुटा है। भारत ने भी अपने एकीकृत स्वास्थ्य सेवा तंत्र में एआई को शामिल कर बीमारी की पहचान, दवाओं की खोज और विकास, व्यक्तिगत उपचार और दूरस्थ रोगी निगरानी और टेलीमेडिसिन आदि में उल्लेखनीय प्रगति की है। इससे साफ है कि एआई की उपयोगिता वैश्विक है और हर प्रकार की स्वास्थ्य प्रणाली में इसके असर देखे जा रहे हैं।
हालांकि, इन तकनीकों के व्यापक और सुरक्षित इस्तेमाल के लिए एक मजबूत और जिम्मेदार नियामक तंत्र की जरूरत है। एआई के जरिए अगर असमानताओं को और बढ़ा दिया गया या वंचित वर्गों को पीछे छोड़ दिया गया, तो यह तकनीक अपने उद्देश्य से भटक सकती है। इसलिए नीति-निर्माताओं, तकनीकी विशेषज्ञों और स्वास्थ्य क्षेत्र के अग्रणी लोगों को मिलकर ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो विकास और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखें।
सीमा-पार सहयोग भी इस दिशा में अहम भूमिका निभा सकता है। साझा प्रयासों और निवेश से एआई अनुसंधान को गति दी जा सकती है, जिससे वैश्विक स्तर पर एक समान और परस्पर जुड़ी हुई स्वास्थ्य प्रणाली बन सके। चीन जैसे देश पहले से ही इस दिशा में अग्रसर हैं। वहां नीति निर्माण में राज्य के साथ-साथ शिक्षाविद्, मध्यम स्तर के अधिकारी और शोधकर्ता भी भाग ले रहे हैं। अब वक्त है कि इसी सोच को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में और आगे बढ़ाया जाए, जहां हर निर्णय सीधा लोगों की जान से जुड़ा होता है।
आखिरकार, स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई की जिम्मेदार, समावेशी और सतर्क शुरुआत न केवल तकनीक की जीत होगी, बल्कि मानवता की भी।
(साभार—चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)
–आईएएनएस