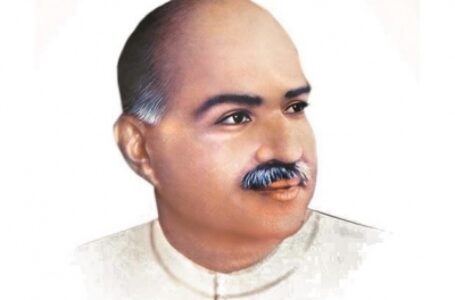देश में इस समय राजद्रोह के अपराध से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए चर्चा में है। ब्रिटिशकाल में स्वतंत्रता सेनानियों का मुंह बंद करने के इरादे से कानून की किताब में शामिल किया गया यह प्रावधान आजादी के बाद भी देश में प्रभावी होने और समय समय पर धारा 124 ए के तहत राजद्रोह का मामला दर्ज किए जाने पर उच्चतम न्यायालय भी चिंतित है।
उच्चतम न्यायालय ने हालांकि अभी तक राजद्रोह के अपराध से संबंधित धारा 124 ए को असंवैधानिक घोषित नहीं किया है लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस प्रावधान की वैधता और आवश्यकता पर नये सिरे से विचार करने का समय आ गया है।
आजादी के बाद भी राजद्रोह के अपराध के आरोप से संबंधित धारा 124 ए को भारतीय दंड संहिता से हटाया नहीं गया है क्योंकि सत्तारूढ़ दलों के लिए सरकार की नीतियों का मुखर होकर विरोध करने वालों का उत्पीड़न करने के लिए यह एक कारगर हथियार है।
राजद्रोह के अपराध से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में कई जनहित याचिकाएं दायर की गयी हैं। इन याचिकाओं में दावा किया गया है कि राजद्रोह के अपराध से संबंधित इस प्रावधान से संविधान में प्रदत्त अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का हनन होता है।
सत्तारूढ़ दलों द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों को सबक सिखाने की मंशा से इस प्रावधान का बार बार कथित रूप से दुरुपयोग होने की घटनाओं के मद्देनजर भारतीय दंड संहिता में इसे अभी तक बनाये रखने के औचित्य पर नये सिरे से विचार की मांग हो रही है।
पहली नजर में यह दावा एकदम सही नजर आता है और न्यायालय भी इसी परिप्रेक्ष्य में धारा 124 ए की संवैधानिक वैधता का परीक्षण कर रहा है। न्यायालय ने इस मामले में केन्द्र सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।
हालांकि, अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल का विचार है कि इसे कानून की किताब में रहने देना चाहिए और लेकिन इसका दुरुपयोग रोकने के लिए न्यायालय दिशा-निर्देश बना सकता है।
इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ने और तेजी से इसका समाधान निकलने में एक समस्या नजर आती है। इस कानून के बारे में उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने जनवरी 1962 में केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार प्रकरण में फैसला सुनाया था। इस फैसले में संविधान पीठ ने कहा था कि राजद्रोह की धाराएं सिर्फ हिंसा भड़काने या सार्वजनिक शांति भंग करने की मंशा जैसे मामलों में ही लगाई जानी चाहिएं। लेकिन सरकार के कार्यों की आलोचना के लिए एक नागरिक के खिलाफ राजद्रोह के आरोप नहीं लगाए जा सकते।
इस फैसले के मद्देनजर सारे मसले पर कम से कम पांच सदस्यीय या फिर सात सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा विचार किये जाने की संभावना है। फिलहाल यह मामला तीन सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष विचाराधीन है।
पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ भाजपा नेता की निजी शिकायत के आधार पर दर्ज प्राथमिकी में अन्य आरोपों के साथ ही राजद्रोह का भी आरोप शामिल था। इस मामले में शीर्ष अदालत ने विनोद दुआ के खिलाफ प्राथमिकी निरस्त करते हुए राजद्रोह के अपराध से संबंधित प्रावधान की भी आलोचना की थी।
इसके बाद ही राजद्रोह से संबंधित कानूनी प्रावधान पर विवाद ने तूल पकड़ा और इसकी संवैधानिक वैधता को नये सिरे से चुनौती दी गयी। इनमे दलील दी गयी है कि ब्रिटिश काल में लागू यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19 (1) में प्रदत्त बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का हनन करता है और केन्द्र तथा राज्य सरकारें लगातार इस प्रावधान का दुरुपयोग कर रही हैं।
इस प्रावधान को चुनौती देने वालों में इंडियन एक्सप्रेस के पूर्व मुख्य संपादक और भाजपा नेता अरुण शौरी, पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेमचा, कन्हैया लाल शुक्ला, ‘द शिलॉन्ग टाइम्स’ की संपादक पेट्रीसिया मुखिम और ‘कश्मीर टाइम्स’ की मालिक अनुराधा भसीन, एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज और मानवाधिकार कार्यकर्ता मेजर-जनरल (अवकाशप्राप्त) एसजी वोम्बटकेरे शामिल हैं। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश के दो तेलुगू समाचार चैनलों- टीवी 5 और एबीएन आंध्र ज्योति के खिलाफ राजद्रोह के आरोप में दर्ज मामला भी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।
हाल ही में जब प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह मामला आया तो न्यायालय भी इसे लेकर चिंतित नजर आया। प्रधान न्यायाधीश भी ‘‘औपनिवेशिक काल’’ के राजद्रोह संबंधी दंडात्मक कानून के ‘‘दुरुपयोग’’ से चिंतित नजर आए।’’ उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘एक गुट के लोग दूसरे समूह के लोगों को फंसाने के लिए इस प्रकार के (दंडात्मक) प्रावधानों का सहारा ले सकते हैं।’’
मामले की सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश ने टिप्पणी की थी कि यदि कोई विशेष पार्टी या लोग (विरोध में उठने वाली) आवाज नहीं सुनना चाहते हैं, तो वे इस कानून का इस्तेमाल दूसरों को फंसाने के लिए करेंगे।
शीर्ष अदालत बार बार कह रही है कि बात-बात पर राजद्रोह की संगीन धाराओं में मुकदमा करने की प्रवृत्ति गलत है और इस पर रोक लगनी चाहिए।
राजद्रोह के कानून के दुरुपयोग पर विधि आयोग ने भी अलग अलग अवसरों पर विचार किया है। आयोग ने न्यायपालिका की चिंताओं से सहमति व्यक्त करते हुए अपनी रिपोर्ट में इस प्रावधान पर पुनर्विचार करने या रद्द का सुझाव भी दिया। लेकिन इसे रद्द करना तो दूर पुनर्विचार तक नहीं हुआ है।
चूंकि राजद्रोह के अपराध से संबंधित धारा 124 ए की संवैधानिक वैधता का सवाल नए सिरे से न्यायालय के सामने आया है और वह भी इसकी समीक्षा करने की जरूरत महसूस करता है, इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए की देर सवेर इस प्रावधान के बारे में शीर्ष अदालत से कोई न कोई उत्साहजनक खबर सुनने को मिलेगी।